Raghuvansh Mahakavya Tritiya Sarg in Hindi
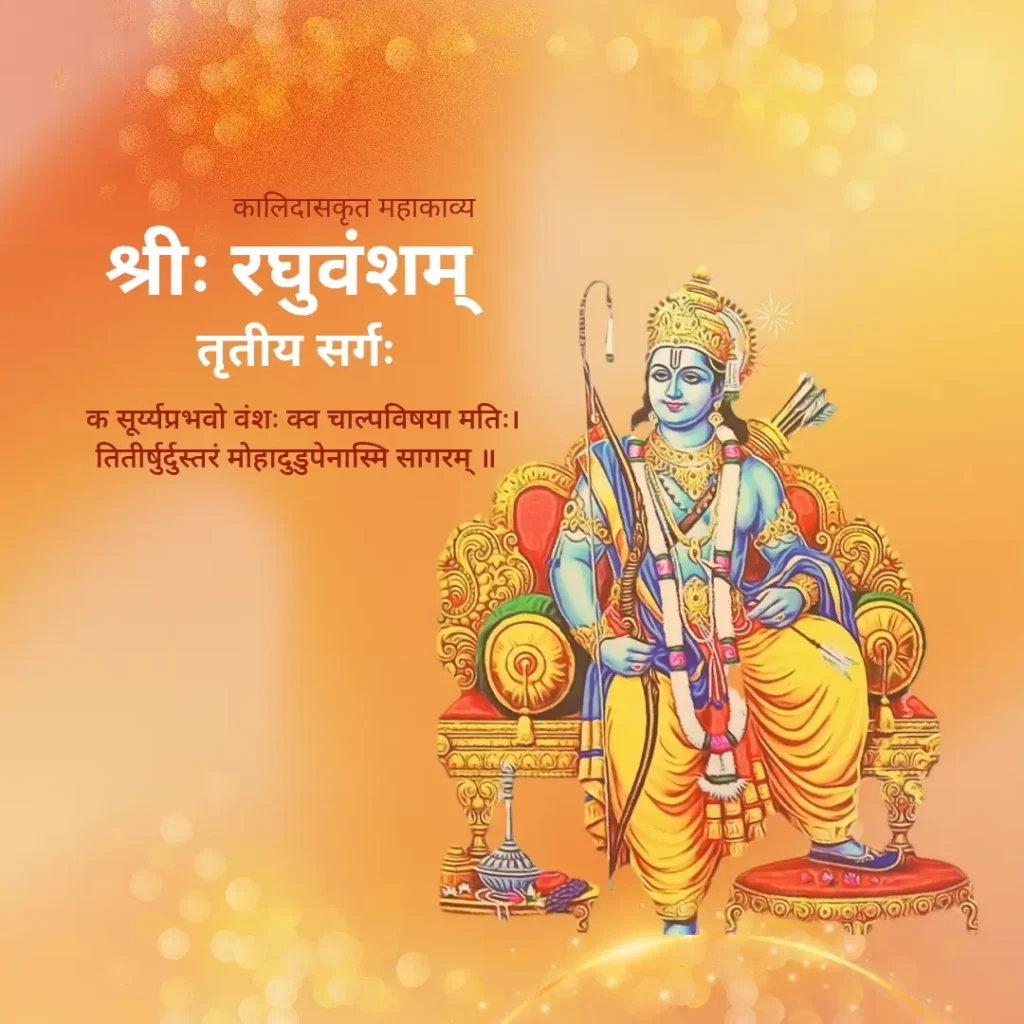
रघुवंशम् महाकाव्य तृतीय सर्ग | Raghuvansham Tritiya Sarg
“रघुवंशम महाकाव्य” (Raghuvansham Tritiya Sarg) महान भारतीय कवि कालिदास द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य है। यह महाकाव्य कालिदास की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, और इसमें उन्नीस सर्ग या “सर्ग” शामिल हैं। “रघुवंशम महाकाव्य” के तीसरे सर्ग में, सुलक्षणा के गर्भ के लक्षण और रघु के जन्म एवं महाराज दिलीप के अश्वमेध यज्ञ की कथा कही गई है।
यहां एक क्लिक में पढ़ें ~ रघुवंशम् महाकाव्य प्रथमः सर्गः
॥ कालिदासकृत रघुवंशम् महाकाव्य तृतीय सर्गः ।।
।। श्रीः रघुवंशम् ।।
अथेप्सितं भर्तुरुपस्थितोदयं सखीजनोद्वीक्षणकौमुदीमुखम् ।
निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य सन्ततेः सुदक्षिणा दोहदलक्षणं दधौ ।।१।।
अर्थ:
अब प्रकट हुए रानी सुदक्षिणा में गर्भलक्षण। वह था पति (दिलीप) का प्रकट हुआ अभीष्ट, सखीजनों की कल्पनाओं का कौमुदीमहोत्सव और इक्ष्वाकुवंश का निदान।
शरीरसादादसमग्र भूषणा मुखेन साऽलक्ष्यत लोध्रपाण्डुना ।
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शर्वरी ॥ २॥
अर्थ:
रानी दुबला गई। वह कुछ ही भूषण धारण करती और उसका चेहरा पड़ गया पीला। उसकी छवि ठीक वैसी ही थी जैसी प्रभात बनने जा रही रात्रि की होती है, जिसमें
शशिबिम्ब का प्रकाश थोड़ा ही शेष रहता है और तारे भी इने गिने।
तदाननं मृत्सुरभि क्षितीश्वरो रहस्युपाघ्राय न तृप्तिमाययौ ।
करीव सिक्तं पृषतैः पयोमुचां शुचिव्यपाये वनराजिपल्लवम् ।। ३ ।।
अर्थ:
(गर्भवती रानी के साथ राजा का शरीरसंपर्क था, परन्तु केवल चुम्बन तक) राजा दिलीप रानी सुदक्षिणा का मिट्टी से सुगन्धित मुख चूम चूम कर अघाते ही नहीं थे, वैसे ही जैसे कोई हाथी ग्रीष्म बीत जाने पर मेघ की पहली बूँदों से सिक्त वनराजिपल्वल (गड्ढे) को सूँघ सैंधकर।
दिवं मरुत्वानिव भोक्ष्यते भुवं दिगन्तविश्रान्तरथो हि तत्सुतः ।
अतोऽभिलाषे प्रथमं तथाविधे मनो बबन्धान्यरसान् विलङ्घय सा ।।४।।
अर्थ:
रानी ने, अन्य सभी रसों को छोड़कर मिट्टी खाना पसंद किया, कदाचित् इस भाव से कि उसका भावी पुत्र पृथिवी का भोग वैसे ही करेगा जैसे इन्द्र द्युलोक का भोग करता है। उसके रथ को विश्राम मिलेगा दिगन्त में। (आसमुद्रधितोशत्व।)
न मे ह्रिया शंसति किंचिदीप्सितं स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी ।
इति स्म पृच्छत्यनुवेलमादृत: प्रियासखी,त्तरकोसलेश्वर: ॥५॥
अर्थ:
उत्तरकोसल (अयोध्या जनपद) के स्वामी दिलीप प्रिया की सखियों से पूछा करते कि रानी सुदक्षिणा मुझसे कुछ भी माँगने में लजा रही है। बतलाओ क्या चाहती है वह?
उपेत्य सा दोहददु:खशीलतां यदेव वव्रे तदपश्यदाहृतम् ।
न हीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदनासाद्यमधिज्यधन्वन: ॥६॥
अर्थ:
गर्भकष्ट में वह (सुदक्षिणा) जो भी चाहती, वह तत्काल उपस्थित पाती। उसके धनुषधारी पति के लिए प्रत्यञ्चा चढ़ा लेने पर रानी की अभीष्ट कोई भी वस्तु स्वर्ग में भी दुर्लभ नहीं थी।(Raghuvansham Tritiya Sarg)
क्रमेण निस्तीर्य च दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा ।
पुराणपत्रापगमादनन्तरं लतेव संनद्धमनोज्ञपल्लवा ॥७॥
अर्थ:
गर्भकष्ट के दिन बीत गए और रानी फिर सम्हलने लगी। इस समय वह उस लता सी लग रही थी जिसके पुराने पत्ने छंट गए हों और जिसमें नई कोपले भर गई हों।
दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमानीलमुखं स्तनद्वयम् ।
तिरश्चकार भ्रमराभिनीलयो: सुजातयो: पङ्कजकोशयो: श्रियम् ॥८॥
अर्थ:
ज्यों-ज्यों दिन चढ़ते गए सुदक्षिणा के आँचर पुष्ट होते गए और जब खूब फूल गए तो उसके अग्रभाग पर श्यामवर्ण छा गया। तब उनसे सुजात और भौरो से लीन कमलकोष की छवि दब गई।
निधानगर्भामिव सागराम्बरां शमीमिवाभ्यन्तरलीनपावकाम् ।
नदीमिवान्त:सलिलां सरस्वतीं नृप: ससत्वां महिषीममन्यत ॥९॥
अर्थ:
परिपूर्ण गर्भवाली उस पत्नी को देखता तो राजा मानता कि यह निधि छिपाई हुई भूमि है, यह भीतर अग्नि लिए शमी है, यह सरस्वती नदी है, पानी भीतर छिपाई हुई।
प्रियानुरागस्य मन: समुन्नतेर्भुजार्जितानां च दिगन्तसंपदाम् ।
यथाक्रमं पुंसवनादिका: क्रिया धृतेश्च धीर: सदृशीव्र्यधत्त स: ॥१०॥
अर्थ:
उसने गर्भवती रानी के पुंसवन आदि सभी विधान क्रम से प्रिया के अनुराग, अपने मन की ऊँचाई और भुजबल से अर्जित दिग्दिगन्तों की सम्पत्ति के ही अनुरूप किए।(Raghuvansham Tritiya Sarg)
सुरेन्द्रमात्राश्रितगर्भगौरवात्प्रयत्नमुक्तासनया गृहागत: ।
तयोपचाराञ्जलिखिन्नहस्तया ननन्द पारिप्लवनेत्रया नृप: ॥११॥
अर्थ:
राजा जब घर लौटता तो रानी उसका स्वागत तो करती, किन्तु वह जो अंजलि बनाती उसमें उसके हाथ कठिनाई से उठ पाते, उसके नेत्र चंचल रहते और वह आसन भी प्रयत्न से ही छोड़ पाती। इसका कारण था गर्भ, जिसमें था सुरेन्द्र की मात्रा से उत्पन्न भार।
कुमारभृत्याकुशलैरनुष्ठिते भिषग्भिराप्तैरथ गर्भभर्मणि ।
पति: प्रतीत: प्रसवोन्मुखीं प्रियां ददर्श काले दिवमभ्रितामिव ॥१२॥
अर्थ:
अब कुमारभृत्या में कुशल प्रामाणिक वैद्यों ने ‘गर्भभर्म’ नामक उपचार पूरा किया और प्रसवोन्मुख प्रिया को आश्वस्त पति (दिलीप) ने प्रतीक्षाभरी आश्वस्त दृष्टि से वैसे ही देखा जैसे समय आने पर अभ्रगर्भित द्यौ को देखा जाता है। (‘कुमारभृत्या’ और ‘गर्भभर्म’ दोनों वैद्यशास्व की परिभाषाएँ हैं। कुमारभृत्या = बालचिकित्सा। गर्भभर्म गर्भ का भरण पोषण।)
ग्रहैस्तत: पञ्चभिरूच्चसंस्थितैरसूर्यगै: सूचितभाग्यसंपदम् ।
असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम् ॥१३॥
अर्थ:
इसके पश्चात् शचीतुल्य रानी ने जन्म दिया पुत्र को, जैसे तीन साधनों वाली शक्ति देती है जन्म अक्षय अर्थ को। जन्म के समय पाँच ग्रह उच्च थे और उन्हें सूर्य नहीं देख रहा था, जिससे उसकी भाग्यसंपत्ति सूचित हो रही थी। (तीन शक्ति प्रभावशक्ति, उत्साहशक्ति, मन्त्रशक्ति ।)
दिश: प्रसेदुर्मरूतो ववु: सुखा: प्रदक्षिणार्चिर्हविरग्निराददे ।
बभूव सर्वं शुभशंसि तत्क्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम् ॥१४॥
अर्थ:
उस समय सभी लक्षण शुभ ही शुभ हो रहे थे। दिशाएँ प्रसन्न (निर्मल) हो उठीं, सुखद वायु बहने लगी और यज्ञाग्नि प्रदक्षिण होकर हविष्य ग्रहण करने लगा। उस जैसों का तो जन्म होता ही है लोकाभ्युदय के लिए।(Raghuvansham Tritiya Sarg)
अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा ।
निशीथदीपा: सहसा हतत्विषो बभूवुरालेख्यसमर्पिता इव ॥१५॥
अर्थ:
उस बालक का जन्म सुखपूर्वक हुआ। चहुँओर फैले उसके अपने तेज से सूतिका गृह की शय्या के आसपास रखे निशीथ दीपक एकाएक हतप्रभ हो उठे। लग रहा था जैसे वे चित्रलिखित दीपक थे। (निशीथ अर्धरात्रि ।
जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्मामृतसंमिताक्षरम् ।
आदेयमासीत्त्रयमेव भूपते: शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे ॥१६॥
अर्थ:
राजा को अन्तःपुर के जिस सेवक ने ‘पुत्रजन्म’ यह अमृततुल्य अक्षरवाला शब्द सुनाया, उसके लिए राजा के पास केवल तीन वस्तुएँ अदेय रह गई थीं चन्द्रमा सा श्वेत छत्र और दो वैसे ही चामर।
निवातद्मस्तिमितेन चक्षुषा नृपस्य कान्तं पिबत: सुताननम् ।
महोदधे: पूर इवेन्दुदर्शनाद्गुरूः प्रहर्ष: प्रबभूव नात्मनि ॥१७॥
अर्थ:
वातरहित सरोवर के पद्म से निश्चल नेत्र से पिया राजा ने पुत्र का कान्तिमान् चेहरा। उससे हुई खुशी उसमें अँट नहीं रही थी, चन्द्रदर्शन से महोदधि के पूर के समान।
स जातकर्मण्यखिले तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते ।
दिलीपसूनुर्मणिराकरो»व: प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ ॥१८॥
अर्थ:
तपस्वी पुरोधा (वसिष्ठ जी) ने तपोवन से आकर पूरा जातकर्म संस्कार संपन्न किया तो दिलीप का वह पुत्र और अधिक सुशोभित हुआ, खरादे जाने पर खदान से निकले मणिरत्न के समान।(Raghuvansham Tritiya Sarg)
सुखश्रवा मङ्गलतूर्यनिस्वना: प्रमोदनृत्यै: सह वारयोषिताम्।
न केवलं सद्मनि मागधीपते: पथि व्यजृम्भन्त दिवौकसामपि ॥१९॥
अर्थ:
उस समय वारवनिताओं के प्रमोदनृत्यों के साथ मंगलतूर्यस्वन गूँज उठे केवल दिलीप के भवन में नहीं, अपितु देवपथ (आकाश) में भी।
न संयतस्तस्य बभूव रक्षितुर्विसर्जयेद्यं सुतजन्महर्षित: ।
ऋणाभिधानात्स्वयमेव केवलं तदा पितäणां मुमुचे स बन्धनात् ॥२०॥
अर्थ:
दिलीप ऐसा रक्षक था कि उसके यहाँ कोई भी बन्दी नहीं था, जिसे वह पुत्रजन्म की खुशी के अवसर पर मुक्ति देता। हाँ, वह स्वयं मुक्त हुआ पितरों के ऋण नामक बन्धन से।
श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भक: तथा परेषां युधि चेति पार्थिव: ।
अवेक्ष्य धातोर्गमनार्थमर्थविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसम्भवम् ॥२१॥
अर्थ:
पिता दिलीप ने अपने पुत्र का नाम रघु (प्रगतिशील) रखा यह देखकर कि आगे चलकर यह एक ओर तो वैदुष्य के अन्तिम बिन्दु तक पहुँचेगा और दूसरी ओर युद्ध में अपने शत्रुओं के भी अन्त तक ‘रघु’ शब्द की प्रकृति ‘रधि’-धातु का गमन अर्थ देखकर रखा था।
पितु: प्रयत्नात्स समग्रसंपद: शुभै: शरीरावयवैर्दिने दिने ।
पुपोष वृद्धिं हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमा: ॥२२॥
अर्थ:
समग्रसंपत्ति वाले पिता (दिलीप) के प्रयत्न से उस बालक के शुभ अंग दिन दिन पुष्ट होते जा रहे थे उसी प्रकार जिस प्रकार बालचन्द्र के अंग सूर्य के अनुप्रवेश से होता है।
उमावृषाङ्कौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ ।
तथा नृप: सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सदृशेन तत्समौ ॥२३॥
अर्थ:
वे दोनों पतिपत्नी, सुदक्षिणा तथा दिलीप उस पुत्र से उसी प्रकार प्रसन्न हुए जिस
प्रकार कार्तिकेय के जन्म से प्रसन्न हुए होंगे पार्वती तथा शङ्कर, या जयन्त के जन्म से शची तथा इन्द्र। राजा-रानी की जोड़ी शिव और पार्वती की जोड़ी तथा शची और इन्द्र की जोड़ी सी ही थी।
रथाङ्कनाम्नोरिव भावबन्धनं बभूव यत्प्रेम परस्पराश्रयम् ।
विभक्तमप्येकसुतेन तत्तयो: परस्परस्योपरि पर्यचीयत ॥२४॥
अर्थ:
उस एक पुत्र के बीच में आ जाने पर भी सुदक्षिणा और दिलीप का चक्रवाक चक्रवाकी सा एक दूसरे पर जो प्रेम था वह बढ़ा ही।
यहां एक क्लिक में पढ़ें ~ श्रीमद भागवत गीता का प्रथम अध्याय
उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गुलिम् ।
अभूच्च नम्र: प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान सोऽर्भक: ॥२५॥
अर्थ:
बालक रघु, धाई जो बोलती उसे बोलता, उसकी उँगली पकड़कर चलता। अभिवादन की शिक्षा से झुक झुककर नम्रता प्रदर्शित करता। इन सबको देख पिता की प्रसन्नता बढ़ती जाती।(Raghuvansham Tritiya Sarg)
तमङ्कमारोप्य शरीरयोगजै: सुखैर्निषिञ्चन्तमिवामृतं त्वचि ।
उपान्तसंमीलितलोचनो नृपश्चिरात्सुतस्पर्शरसज्ञतां ययौ ॥२६॥
अर्थ:
राजा को सुतस्पर्श के सुख का अनुभव बड़ी देरी से हुआ। राजा पुत्र को गोद में बिठाता और सुख का अनुभव करता। वह (पुत्र) त्वचा पर मानों अमृत सोंचता। सुखानुभव से उस (दिलीप) की आखों के छोर संकुचित हो जाते।
अमंस्त चानेन पराध्र्यजन्मना स्थितेरभेत्ता स्थितिमन्तमन्वयम् ।
स्वमूर्तिभेदेन गुणाग्यवर्तिना पति: प्रजानामिव सर्गमात्मन: ॥२७॥
अर्थ:
मर्यादास्थापक दिलीप ने अपने वंश को इस पुत्र से अस्तित्वयुक्त माना। क्यों नहीं, इसका जन्म सर्वोत्कृष्ट जो था। ऐसा ही माना था प्रजापति ने अपनी ही सत्त्वगुणी मूर्ति (विष्णु) से अपनी सृष्टि को। (सत्त्वगुणी मूर्ति- विष्णु, वल्लभ, हेमाद्रि मल्लिनाथ, दिनकर, अरुणगिरिनाथ, नारायण, दक्षादिप्रजापति अधिक उपयुक्त। अभेता-स्थापक अरुणगिरिनाथ)
स वृत्तचूलश्चलकाकपक्षकैरमात्यपुत्रै: सवयोभिरन्वित: ।
लिपेर्यथावद्ग्रहणेन वा¨यं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत् ॥२८॥
अर्थ:
अब हुआ उस बालक का चूडाकर्म संस्कार। उसी के साथ चूडाकर्म हुआ समान वय के अमात्यपुत्रों का। उन सबके साथ रघु का हुआ विद्यारम्भ संस्कार। पहले उसने सीखी विधिवत् लिपि। तब प्रवेश किया वाड्मय में, वैसे ही जैसे नदीमुख से समुद्र में प्रवेश कर लिया जाता है।
अथोपनीतं विधिवद्विपश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गु,प्रियम् ।
अवन्ध्ययत्नाश्च बभूवुरत्र ते क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति ॥२९॥
अर्थ:
अब हुआ रघु का विधिवत् उपनयन संस्कार। इसके पश्चात् विद्वान् गुरुजनों ने गुरुप्रिय उसे शिक्षा (विनय) देना आरम्भ किया और वे अपने यत्न में सफल रहे। शिक्षा में प्रसाद आता ही योग्य शिष्य में पहुँचकर। (क्रिया-शिक्षा कौटल्य, वस्तु-कुशाग्रबुद्धि)।
धिय: समग्रै: स गुणै,दारधी: क्रमाच्चतस्रश्चतुरर्णवोपमा: ।
ततार विद्या: पवनातिपातिभिर्दिशो हरिद्भिर्हरितामिवेश्वर: ॥३०॥
अर्थ:
धीरे धीरे चार समुद्रों सी चारों विद्याएँ (आन्वीक्षिकी, त्रयौ, वार्ता, दण्डनीति) पार कर गया रघु। उसी प्रकार जिस प्रकार पवन वेग से तीव्र वेग वाले अश्वों से सूर्य पार कर जाता है दिगन्तरालों को रघु की बुद्धि में सभी (सातों गुण जो थे और वह उदारधी था)। (सात गुण- शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, अर्थविज्ञान और तत्वज्ञान। ऊहापोह को मिलाकर गिना गया।)
त्वचं च मेध्यां परिधाय रौरवीमशिक्षतास्त्रं पितुरेव मन्त्रवत् ।
न केवलं तद्भुरेकपार्थिव: क्षितावभूदेकधनुर्धरोऽपि स: ॥३१॥
अर्थ:
अब सीखी उसने शस्त्रविद्या। उसने पवित्र मृगचर्म धारण किया और अपने पिता से ही ग्रहण की शस्त्रविद्या। उसका पिता केवल अद्वितीय राजा ही नहीं था। वह पूरे पृथिवीलोक पर अद्वितीय धनुर्विद्याविशारद भी था।(Raghuvansham Tritiya Sarg)
महोक्षतां वत्सतर: स्पृशन्निव द्विपेन्द्रभावं कलभ: श्रयन्निव ।
रघु: क्रमाद्यौवनभिन्नशैशव: पुपोष गाम्भीर्यमनोहरं वपु: ॥३२॥
अर्थ:
अब रघु युवक हो गया, वैसे ही जैसे छोटा सा बच्छा महोक्ष बन जाता है या करिशावक बन जाता है गजराज। रघु का शैशव बीता और यौवन ने उसके शरीर में पुष्टि, गाम्भीर्य और मनोहारिता ला दी।
अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवर्तयद्गुरूः ।
नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पतिं तमोनुदं दक्षसुता इवाबभु: ॥३३॥
अर्थ:
फिर हुआ रघु का गोदान (मुण्डन) संस्कार। पश्चात्वि वाह। अनेक राजकन्याएँ रघु जैसा सत्पति पाकर उसी प्रकार सुशोभित हुईं जैसे तमोहारी (चन्द्र) को पति के रूप में प्राप्त कर सुशोभित हुई थी प्रजापति दक्ष की पुत्रियाँ। (गो केश, दान-काटना। ‘दो अवखण्डने’ धातु।)
युवा युगव्यायतबाहुरंसल: कवाटवक्षा: परिणद्धकंधर: ।
वपु:प्रकर्षादजयद्गुरूं रघुस्तथापि नीचैर्विनयाददृश्यत ॥३४॥
अर्थ:
यौवन आते ही रघु के बाहु युग (जुए) से लम्बे हो गए। कन्धों पर पुष्टि आ गई वक्षःस्थल (किले के मुख्य द्वार के) किवाड़ों सा फैल गया और ग्रीवा भर गई। इस प्रकार शरीर के प्रकर्ष में वह अपने पिता से आगे था, किन्तु विनय के कारण छोटा ही दिखाई देता था।
तत: प्रजानां चिरमात्मना धृतां नितान्तगुर्वीं लघयिष्यता धुरम् ।
निसर्गसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक् ॥३५॥
अर्थ:
इसके पश्चात् राजा ने रघु को युवराज का ओहदा दे दिया। यह इस कारण कि उसमें विनय का संस्कार स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित था और अब लम्बे अर्से से सम्हाले प्रजापालन के बोझ को राजा हल्का करना चाहता था।
नरेन्द्रमूलायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रीर्युवराजसंज्ञितम् ।
अगच्छदंशेन गुणाभिलाषिणी नवावतारं कमलादिवोत्पलम् ॥३६॥
अर्थ:
गुणों को चाहती राजलक्ष्मी वृद्ध पिता के पास से युवा पुत्र में आंशिक रूप से संक्रान्त हुई तो वैसे ही बड़ी अच्छी लगी जैसे कमल से नए खिले उत्पल पर संक्रान्त श्री (शोभा) अच्छी लगती है।
विभावसु: सारथिनेव वायुना घनव्यपायेन गभस्थिमानिव ।
बभूव तेनातितरां सुदु:सह: कटप्रभेदेन करीव पार्थिव: ॥३७॥
अर्थ:
राजा दिलीप युवराज रघु की शक्ति से और अधिक दुःसह हो गए, वैसे ही जैसे वायु को सारथि पा अग्नि हो जाया करता है, शरद् ऋतु के योग से सूर्य और कटप्रभेद से (मदधारा फूट पड़ने पर) गजराज।(Raghuvansham Tritiya Sarg)
नियुज्य तं होमतुरंगरक्षणे धनुर्धरं राजसुतैरनुद्रुतम् ।
अपूर्णमेकेन शतक्रतूपम: शतं क्रतूनामपविघ्नमाप स: ॥३८॥
अर्थ:
इसके पश्चात् राजा दिलीप ने, राजपुत्रों के साथ रघु के संरक्षण में होमतुरंग को स्वच्छन्द छोड़कर, निन्यानवे अश्वमेध तो कर लिए, उनमें कोई बाधा नहीं आई।
तत: परं तेन मखाय यज्वना तुरंगमुत्सृष्टमनर्गलं पुन: ।
धनुर्भृतामग्रत एव रक्षिणां जहार शक्र: किल गूढविग्रह: ॥३९॥
अर्थ:
परन्तु जब सौवाँ अश्वमेध करने हेतु अश्व छोड़ा तो सभी धनुषधारी रक्षकों के देखते देखते ही उस (अश्व) को अदृश्य इन्द्र ने हरण कर लिया।
विषादलुप्तप्रतिपत्ति विस्मितं कुमारसैन्यं सपदि स्थितं च तत् ।
वसिष्ठधेनुश्च यदृइच्छयागता श्रुतप्रभावा ददृशेऽथ नन्दिनी ॥४०॥
अर्थ:
(उसी समय हुआ चमत्कार) कुमार-सेना विषाद में डूब गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एकाएक उपस्थित दिखाई दी वसिष्ठधेनु (नन्दिनी) जिसका प्रभाव सुना जा चुका है (सर्ग-२ में)।
तदङ्कनिस्यन्दनजलेन लोचने प्रमृज्य पुण्येन पुरस्कृत: सताम् ।
अतीन्द्रियेष्वप्युपपन्नदर्शनो बभूव भावेषु दिलीपनन्दन: ॥४१॥
अर्थ:
रघु ने उसकी पवित्र गुमातर से आँखें धोई और सत्पुरुषों में अग्रगण्य उसकी दृष्टि में आ गई शक्ति अतीन्द्रिय पदार्थों को भी देख लेने की।
स पूर्वत: पर्वतपक्षशातनं ददर्श देवं नरदेवसंभव: ।
पुन: पुन: सूतनिषिद्धचापलं हरन्तमश्वं रथरश्मिसंयुतम् ॥४२॥
अर्थ:
उसे दिखाई दिया कि पूर्व दिशा में इन्द्र रथ के पीछे रस्सी से बाँध कर लिए जा रहा है अश्व को और उसकी चपलता को सूत बारम्बार रोक रहा है।
शतैस्तमक्ष्णामनिमेषवृत्तिभिर्हरिं विदित्वा हरिभिश्च वाजिभि: ।
अवोचदेनं गगनस्पृशा रघु: स्वरेण धीरेण निवर्तयन्निव ॥४३॥
अर्थ:
निमेषरहित हजार नेत्रों से और घोड़ों के हरित् (नई) रंग से रघु ने समझ लिया कि यह देवराज इन्द्र हैं, तो गंभीर गगनस्पर्शी स्वर में उन्हें लौटाते हुए सा कहा।
मखांशभाजां प्रथमो मनीषिभिस्त्वमेव देवेन्द्र सदा निगद्यसे ।
अजस्रदीक्षाप्रयतस्य मद्गुरो: क्रियाविघाताय कथं प्रवर्तसे ॥४४॥
अर्थ:
हे देवराज! मनीषीजन आपको ही तो मानते हैं प्रथमतम मखांशभागी। तब यह क्या कि आप ही बन रहे हैं विघ्न मेरे निरन्तर यज्ञरत पिता के यज्ञानुष्ठान में आप ही तो हैं तीनों लोकों के स्वामी है।
त्रिलोकनाथेन सदा मखद्विषस्त्वया नियम्या ननु दिव्यचक्षुषा ।
स चेत्स्वयं कर्मसु धर्मचारिणां त्वमन्तरायो भवसि च्युतो विधि: ॥४५॥
अर्थ:
आपका ही तो है दायित्व यज्ञशत्रुओं पर नियंत्रण का। आप ही यदि विघ्न बनेंगे धर्मानुष्ठान करने में लगे सत्पुरुषों के अनुष्ठान में तो फिर नष्ट है सारी विधि।
तदङ्कमग्यं मघवन्महाक्रतोरमुं तुरंगं प्रतिमोक्तुमर्हसि ।
पथ: श्रुतेर्दर्शयितार ईश्वरा मलीमसामददते न पद्धतिम् ॥४६॥
अर्थ:
इसलिए हे अङ्ग। उचित है कि महाक्रतु के अंग इस अश्व को आप छोड़ दें। श्रुति मार्ग के दर्शक और समर्थ जन कलुषित मार्ग नहीं अपनाया करते।
इति प्रगल्भं रघुणा समीरितं वचो निशम्याधिपतिर्दिवौकसाम् ।
निवर्तयामास रथं सविस्मय: प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुमुत्तरम् ॥४७॥
अर्थ:
रघु के ऐसे प्रगल्भ वचन सुने तो देवताओं के अधिपति (इन्द्र) को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने रथ लौटाकर उत्तर देना आरम्भ किया।(Raghuvansham Tritiya Sarg)
यदात्थ राजन्यकुमार तत्तथा यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनै: ।
जगत्प्रकाशं तदशेषमिज्यया भवद्गुरूर्लङ्घयितुं ममोद्यत: ॥४८॥
अर्थ:
हे राजन्य (क्षत्रिय) कुमार! तुमने जो कहा वह ठीक है, परन्तु यश की रक्षा करना तो प्रत्येक यशोधन का कर्त्तव्य है, विशेषतः दूसरे व्यक्ति से। तुम्हारे पिता मेरे उसी जगत्प्रसिद्ध यश को यज्ञ पूर्ण कर क्षति पहुँचाने जा रहे थे।
हरिर्यथैक: पु,षोत्तम: स्मृतो महेश्वरस्त्र्यम्बक एव नापर: ।
तथा विदुर्मां मुनय: शतक्रतुं द्वितीयगामी न हि शब्द एष न: ॥४९॥
अर्थ:
जैसे ‘पुरुषोत्तम’ एकमात्र विष्णु कहलाते हैं, दूसरा कोई नहीं और जैसे त्र्यम्बक केवल महेश्वर अन्य कोई नहीं वैसे ही ‘शतक्रतु’ नाम से मुनिजन केवल मुझे ही जानते हैं। हमारा यह शब्द किसी और के लिए प्रयुक्त नहीं होता।
अतोऽयमश्व: कपिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मयापहारित: ।
अलं प्रयत्नेन तवात्र मा निधा: पदं पदव्यां सगरस्य संतते: ॥५०॥
अर्थ:
इस कारण तुम्हारे पिता का यह अश्व मैंने पकड़वा लिया जैसे कभी कपिल (राक्षस) ने पकड़वाया था। तुम्हारे प्रयत्न से कुछ होने वाला नहीं, फलतः सगरपुत्रों के पथ पर पैर मत रखो। (सगर का यज्ञाश्व कपिल नामक राक्षस ने चुराकर पाताल में कपिल महर्षि के पास बाँध दिया था। सगर के सौ पुत्र अश्व की खोज में वहाँ पहुँचे और तपोरत महर्षि को भलाबुरा कहने लगे। उनकी समाधि टूटी तो उनके नेत्र की ज्वाला में सब भस्म हो गए। उनका उद्धार तब हुआ जब भगीरथ और अंशुमान् ने घोर तपकर गङ्गा को स्वर्ग से पृथिवी पर उतारा और वह पहुँची ‘भोगावती’ नाम से पाताल लोक। अश्व कपिल मुनि के पास बंधा था तो सगर-पुत्रों ने यही सोचा कि उसका अपहरण उन्होंने किया या कराया है।)
तत: प्रहास्यापभय: पुरन्दरं पुनर्बभाषे तुरगस्य रक्षिता ।
गृहाण शस्त्रं यदि सर्ग एष ते न खल्वनिर्जित्य रघुं कृती भवान् ॥५१॥
अर्थ:
रघु हँसा और निर्भीक होकर उसने इन्द्र को चुनौती दी उदाइए अस्त्र यदि यही निश्चय है आपका। रघु को जीते बिना आप सफल नहीं होंगे, उस पर अश्वरक्षा का दायित्व जो था।
स एवमुक्त्वा मघवन्तमुन्मुख: करिष्यमाण: सशरं शरासनम् ।
अतिष्ठदालीढविशेषशोभिना वपु:प्रकर्षेण विडम्बितेश्वर: ॥५२॥
अर्थ;
रघु ऐसा कहकर इन्द्र की ओर हो धनुष पर बाण का सन्धान करने लगा उसने जो आलीढ-मुद्रा अपनाई उससे वह ऐसा लगा जैसे कभी भगवान् शङ्कर लगे थे। आलीढमुद्रा दाहिना पैर पीछे खींचकर बााँ घुटना उठाए रखना।
रघोरवष्टम्भमयेन पत्रिणा हृदि क्षतो गोत्रभिदप्यमर्षण: ।
नवाम्बुदानीकमुहूर्तलाञ्छने धनुष्यमोघं समधत्त सायकम् ॥५३॥
अर्थ:
रघु के सुवर्णजटित बाण से इन्द्र का वक्षःस्थल घायल हो गया तो नए मेघों पर कुछ देर तक दिखाई देने वाले अपने धनुष पर इन्द्र ने भी अमोघ बाण चढ़ाया। उन्हें क्रोध आ गया था।(Raghuvansham Tritiya Sarg)
दिलीपसूनो: स बृहद्भुजान्तरं प्रविश्य भीमासुरशोणितोचित: ।
पपावनास्वादितपूर्वमाशुग: कुतूहलेनेव मनुष्यशोणितम् ॥५४॥
अर्थ:
भयंकर असुरों के रक्त के पान का अभ्यासी वह बाण दिलीपपुत्र (रघु) के विशाल वक्षःस्थल में आ भैंसा और उसने पहली बार पान किया तब तक अनचखे मनुष्य रक्त का, एक प्रकार से कुतूहल में आकर।
हरे: कुमारोऽपि कुमारविक्रम: सुरद्विपास्फालनकर्कशाङ्गुलौ ।
भुजे शचीपत्रविशेषकाङ्किते स्वनामचिह्नं निचखान सायकम् ॥५५॥
अर्थ:
कार्त्तिकेय जैसे पराक्रमी कुमार ने भी चलाया बाण। वह जाकर चुभा इन्द्र की भुजा में, ऐरावत का माँथा थपथपाने से जिसकी उँगलिया कर्कश थों और जिस पर इन्द्राणी ने अपने हाथ से पत्रविशेषक का मण्डन बना रखा था। हाँ। उस बाण में रघु का अपना नाम खुदा था।
जहार चान्येन मयूरपत्रिणा शरेण शक्रस्य महाशनिध्वजम् ।
चुकोप तस्मै स भृशं सुरश्रिय: प्रसत्द्य केशव्यपरोपणादिव ॥५६॥
अर्थ:
रघु ने एक बाण और चलाया जिसमें लगे थे मोर पंख। उसने काट डाली इन्द्र की वज्ज्ञांकित ध्वजा। उससे इन्द्र बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसे लगा कि एक प्रकार से सुरलक्ष्मी के केश किसी ने काट लिए। (स्वी का मुण्डन उसके वैधव्य का सूचक होता है।)
तयो,पान्तस्थितसिद्धसैनिकं गरूत्मदाशीविषभीमदर्शनै: ।
बभूव युद्धं तुमुलं जयैषिणोरधोमुखैरूध्र्वमुखैश्च पत्रिभि: ॥५७॥
अर्थ:
इस युद्ध में एक ओर (इन्द्र के पास) खड़े थे सिद्धपुरुष और दूसरी ओर (रघु के पास) सैनिक। दोनों के बाण, पंखधारी सपों से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चल रहे थे। युद्ध तुमुल था। एक दूसरे, एक दूसरे को चाह रहे थे जीत लेना।
अतिप्रबन्धप्रहितास्त्रवृष्टिभिस्तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य तेजस: ।
शशाक निर्वापयितुं न वासव: स्वतश्र्युतं वह्निमिवाद्भिरम्बुद: ॥५८॥
अर्थ:
रघु का तेज नितान्त असह्य था। उस पर इन्द्र ने बाणों की घनघोर वर्षाएँ की, परन्तु वे उसे शान्त कर नहीं पाए, मेघ भी खुद से उत्पन्न अग्नि (विद्युत्) को नहीं बुझा पाता।
तत: प्रकोष्ठे हरिचन्दनाङ्किते प्रमथ्यमानार्णवधीरनादिनीम् ।
रघु: शशाङ्कार्धमुखेन पत्रिणा शरासनज्यामलुनाद्विडौजस: ॥५९॥
अर्थ:
यह तो पिता पुत्र की लड़ाई थी। आगे बढ़कर रघु ने अर्धचन्द्र बाण छोड़ा जिसने काट डाली इन्द्र के धनुष की वह प्रत्यञ्चा जो इन्द्र के हरिचन्दनाकित मणिबन्ध में मथे जा रहे समुद्र सी ध्वनि उगल रही थी।
स चापमुत्सृज्य विवृद्धमत्सर: प्रणाशनाय प्रबलस्य विद्विष: ।
महीध्रपक्षव्यपरोपणोचितं स्फुरत्प्रभामण्डलमस्त्रमाददे ॥६०॥
अर्थ:
इन्द्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने चाप फेंका और शत्रु (रघु) को मौत के घाँट उतारने हेतु वह अस्व (वज) धनुष पर चढ़ाया जिससे काटे जाते रहे थे पर्वतों के पंख और जिसके आसपास बना था स्फुरित कान्ति का मण्डल।
रघुर्भृशं वक्षसि तेन ताडित: पपात भूमौ सह सैनिकाश्रुभि: ।
निमेषमात्रादवधूय च व्यथां सहोत्थित: सैनिकहर्षनिस्वनै: ॥६१॥
अर्थ:
उससे रघु के वक्ष पर बहुत ही गहरी चोट पहुँची। वह सैनिकों के अश्रुओं के साथ भूमि पर गिरा, किन्तु पल झपकते ही उठ खड़ा हुआ सैनिको की हर्ष ध्वनि के साथ।
तथापि शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे विपक्षभावे चिरमस्य तस्थुष: ।
तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रहा पदं हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते ॥६२॥
अर्थ:
इतने पर भी रघु निष्ठुरतापूर्वक चलाता ही जा रहा था शस्व। इसके इस निरतिशय वीर्य से इन्द्र को बड़ा तोष मिला, जबकि वह वृत्र से शत्रु को मार चुका था। क्यों नहीं, गुण सभी जगह अपना स्थान बना ही लेते हैं।
असङ्गमद्रिष्वपि सारवत्तया न मे त्वदन्येन विसोढमायुधम् ।
अवेहि मां प्रीतमृते तुरङ्गमात्किमिच्छसीति स्फुटमाह वासव: ॥६३॥
अर्थ:
वे स्पष्ट रूप से बोले ‘मेरा यह अस्त्र मारक क्षमता में इतना बड़ा है कि यह पर्वतों पर भी कभी विफल नहीं हुआ। इसे तुम्हें छोड़ अभी तक कोई भी सह नहीं सका। मैं तुम पर खुश हूँ। इस यज्ञाश्व को छोड़, जो चाहो माँग लो।(Raghuvansham Tritiya Sarg)
ततो निषङ्गादसमग्रमुधृतं सुवर्णपुङ्खद्युतिरञ्जिताङ्गुलिम् ।
नरेन्द्रसूनु: प्रतिसंहरन्निषुं प्रियंवद: प्रत्यवदत्सुरेश्वरम् ॥६४॥
अर्थ:
इसके बाद प्रियंवद राजकुमार रघु इन्द्र से बोले। उन्होंने निषङ्ग से अधखिंचे बाण को वापस किया। बाण के पुंख थे सुवर्ण के, जिनकी कान्ति से रघु को उँगलियाँ पीली पड़ गई थी।
अमोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो तत: समाप्ते विधिनैव कर्मणि ।
अजस्रदीक्षाप्रयत: स मद्गुरूः क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम् ॥६५॥
अर्थ:
‘प्रभो! यदि आप अश्व नहीं छोड़ना चाहते तो ऐसा वर दीजिए कि यज्ञकर्म में निरन्तर निरत मेरे पिताजी यज्ञकर्म की विधि अधूरी रहने पर भी यज्ञ का पूरा फल पा लेवें।
यथा स वृत्तान्तमिमं सदोगतस्त्रिलोचनैकांशतया दुरासद: ।
तवैव संदेशहराद्विशांपति: शृणोति लोकेश तथा विधीयताम् ॥६६॥
अर्थ:
हे लोकेश! एक प्रार्थना और कि इस घटना की सूचना पिताजी के पास आपका ही कोई दूत पहुँचा दे, क्योंकि वे यज्ञ में दीक्षित, अतएव अष्टमूर्ति शिव की एक (उम्र नामक) मूर्ति है। उनके पास मनुष्य का पहुँचना कठिन है।’
तथेति कामं प्रतिशुश्रुवान्रघोर्यथागतं मातलिसारथिर्ययौ ।
नृपस्य नातिप्रमना: सदोगृहं सुदक्षिणासूनुरपि न्यवर्तत ॥६७॥
अर्थ:
इन्द्र ने ‘तथा’ कहकर रघु की प्रार्थना को स्वीकृति दी। सारथि मातलि के साथ वे उसी रास्ते लौट गए जिससे आए थे। सुदक्षिणा-सूनु (रघु) भी राजा दिलीप की यज्ञशाला पहुँचे। वे अधिक प्रसन्न नहीं थे।
तमभ्यनन्दत्प्रथमं प्रबोधित: प्रजेश्वर: शासनहारिणा हरे: ।
परामृशन्हर्षजडेन पाणिना तदीयमङ्गं कुलिशव्रणाङ्कितम् ॥६८॥
अर्थ:
दिलीप को पहले ही इन्द्र के संदेशवाहक ने सारी सूचना दे दी थी। उन्होंने पुत्र (रघु) का अभिनन्दन किया वज्रधात के व्रण से अंकित उसके शरीर पर प्रसन्नता से शीतल हाथ फेरते हुए।
इति क्षितीशो नवतिं नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासन: ।
समारूरूक्षुर्दिवमायुष: क्षये ततान सोपानपरम्परामिव ॥६९॥
अर्थ:
इस प्रकार राजा महनीय शासन वाले दिलीप ने निन्यानवे महाक्रतुओं की सीढ़ी सी फैला दी आयुष्य समाप्त होने पर स्वर्ग तक चढ़ने हेतु।
वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है?
अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे
नृपतिककुदं दत्वा यूने सितातपवारणम् ।
मुनिवनतरूच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलव्रतम् ॥७०॥
अर्थ:
दिलीप का चित्त (आत्मा) अब विषयों से लौटा। उसने राजा का चिह्न, श्वेतवर्ण का छत्र, युवक पुत्र रघु को विधिवत् प्रदान कर दिया और स्वयं उस रानी (सुदक्षिणा) के साथ जा बैठा मुनिवनतरुओं के नीचे। उमर ढलने पर इक्ष्वाकुवंशीय प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करते आये हैं। उनका यही रहा है कुलव्रत।(Raghuvansham Tritiya Sarg)
तृतीय सर्ग (Raghuvansham Tritiya Sarg) कथा
उत्तराधिकारी की लालसा में राजा दिलीप ने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए, जिनमें पुंसवन (एक लड़का सुनिश्चित करने का समारोह) और सीमंतोन्नयन (गर्भावस्था के दौरान एक अनुष्ठान) शामिल थे। ये अनुष्ठान शाही पुजारियों द्वारा बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ किए जाते थे।
जब शुभ समय आया तो राजा अपने पुत्र के जन्म की खबर सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। शाही पुजारी वशिष्ठ ने आवश्यक जन्म अनुष्ठान आयोजित किए, और राजा दिलीप ने बच्चे का नाम “रघु” रखा। रघु, चंद्रमा की तरह, तेजी से विकसित हुआ और थोड़े ही समय में सभी कलाओं और विज्ञानों में उत्कृष्ट हो गया।
एक युवा व्यक्ति के रूप में, राजा दिलीप ने रघु को युवराज नियुक्त किया और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान, सौवें अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की। रघु को यज्ञ के घोड़े की रक्षा करने और सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने की खोज, दिग्विजय पर निकलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
अपनी यात्रा के दौरान, स्वर्ग के राजा और हिंदू पौराणिक कथाओं में देवता, इंद्र, रघु की बढ़ती शक्ति और कद के बारे में चिंतित हो गए। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर रघु की वीरता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जैसे ही रघु और उनके रक्षकों ने इंद्र की शक्ति का सामना किया, नंदिनी नाम की एक दिव्य गाय घटनास्थल पर प्रकट हुई।
रघु ने अपनी आंखों को साफ करने के लिए नंदिनी के मूत्र का उपयोग किया, जिससे उन्हें दिव्य शक्ति और दृष्टि मिली। तब वह देवता को युद्ध के लिए चुनौती देते हुए, इंद्र का सामना करने में सक्षम था। एक भयंकर युद्ध हुआ और रघु ने तीर चलाए जिससे इंद्र की बांह कट गई और उनके रथ पर विजय का प्रतीक ध्वज कट गया।
रघु की वीरता से प्रभावित होकर इन्द्र चुराया हुआ घोड़ा लौटाने को तैयार हो गये। उन्होंने रघु को एक वरदान भी दिया, जिससे वह कोई भी इच्छा माँग सकता था। रघु ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए घोड़े को वापस लौटाने का अनुरोध किया और अश्वमेध यज्ञ के गुणों में हिस्सा मांगा।
इंद्र रघु के अनुरोध पर सहमत हुए और आशीर्वाद के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। इस युद्ध में इंद्र पर रघु की वीरतापूर्ण विजय ने उनकी वीरता और धार्मिकता को प्रदर्शित किया।
तृतीया सर्ग रघु के असाधारण गुणों पर प्रकाश डालता है और रघु वंश की महानता का पूर्वाभास देता है, जिसमें भगवान राम भी शामिल हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं। यह सर्ग “रघुवंशम महाकाव्य” का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्राचीन भारत में गुणी और वीर राजाओं की वंशावली का जश्न मनाता है।
॥ इति श्रीकालिदासकृते रघुवंशे महाकाव्ये राज्याभिषेको नाम तृतीय: सर्ग: ॥
इस प्रकार महाकवि कालिदास कृति रघुवंश महाकाव्य में पूरा हुआ रघुराज्याभिषेक नामक तृतीय सर्ग ।। ३।।
यह भी पढ़े
श्री योग वासिष्ठ महारामायण हिंदी में
श्री राम रक्षा स्तोत्रम् हिंदी में


 Download the Mahakavya App
Download the Mahakavya App