Chanakya Niti chapter 7 In Hindi
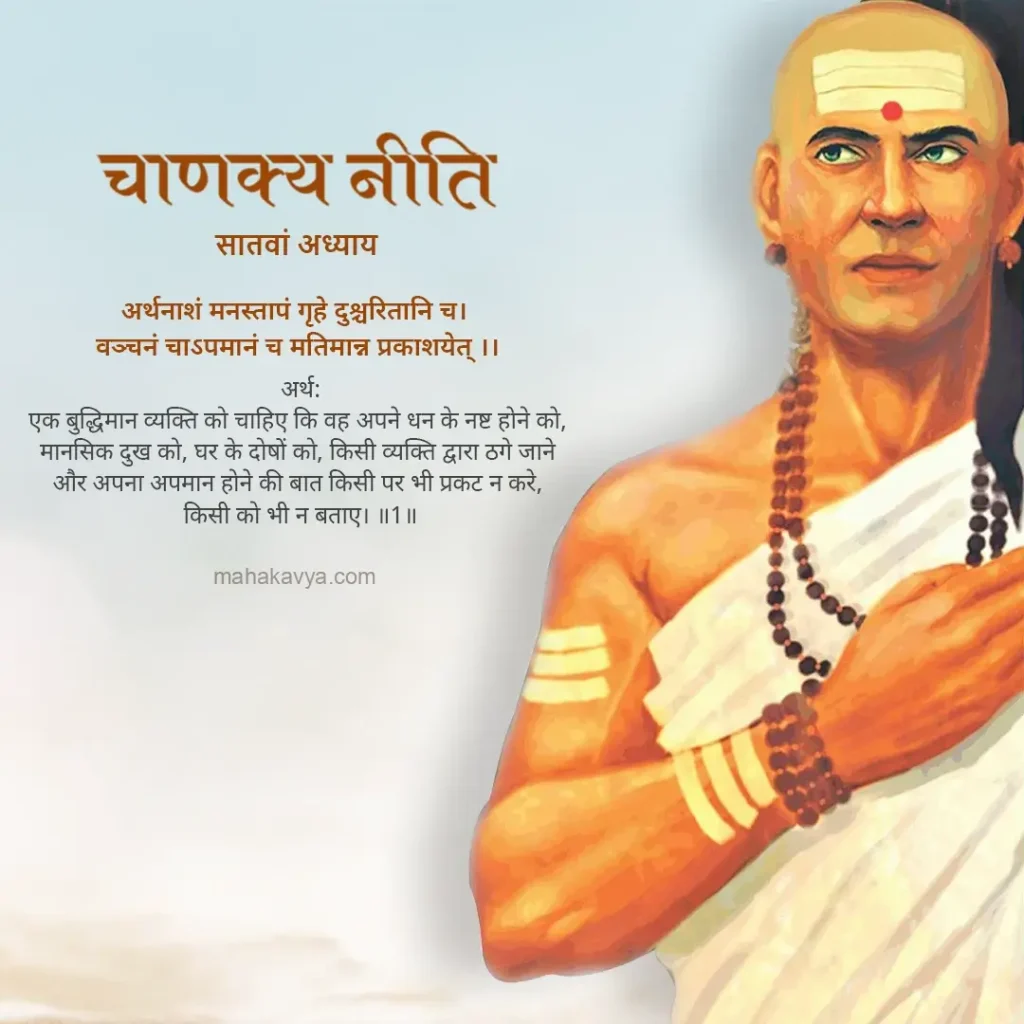
चाणक्य नीति : अध्याय सातवां | Chanakya Niti Chapter 7 In Hindi
॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥
चाणक्य नीति के सातवें अध्याय (Chanakya Niti chapter 7) में चाणक्य यह महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जिस मनुष्य ने विद्या को ग्रहण नहीं किया, उसका जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है, जिससे न तो वह अपने गुप्त भागों को ढंक सकता है, न ही काटने वाले मच्छर आदि कीटों को उड़ा सकता है।
चाणक्य सातवें अध्याय (Chanakya Niti chapter 7) में विद्या (शिक्षा और ज्ञान) के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य विद्या अर्जित नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। वे इसे एक कुत्ते की पूंछ से तुलना करते हैं, जो न तो किसी उपयोग की होती है और न ही किसी समस्या का समाधान कर सकती है।
इसका गहरा अर्थ यह है कि बिना शिक्षा और ज्ञान के मनुष्य जीवन में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। अशिक्षित व्यक्ति न तो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है और न ही समाज में सम्मान प्राप्त कर सकता है।
यह नीति हमें यह सिखाती है कि विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, जो उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सम्मान दिलाती है।
यदि आप सम्पूर्ण चाणक्य नीति पढ़ना चाहते है, तो कृपया यहां क्लिक करे ~ सम्पूर्ण चाणक्य नीति
सातवां अध्याय
अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च।
वञ्चनं चाऽपमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत् ॥
अर्थ:
एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपना अपमान होने की बात किसी पर भी प्रकट न करे, किसी को भी न बताए ॥1॥
प्रत्येक व्यक्ति को कभी-न-कभी धन की हानि उठानी पड़ती है, उसके मन में किसी प्रकार का दुख या संताप भी हो सकता है। प्रत्येक घर में कोई-न-कोई बुराई भी होती है। कई बार उसे धोखा देकर ठगा जाता है और किसी के द्वारा उसे अपमानित भी होना पड़ सकता है, परंतु समझदार व्यक्ति को चाहिए इन सब बातों को वह अपने मन में ही छिपाकर रखे, इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रकट न करे। जानकर लोग हंसी ही उड़ाते हैं। ऐसी स्थिति में वह स्वयं उनका मुकाबला करे और सही अवसर की तलाश करता रहे।(Chanakya Niti chapter 7)
धन-धान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च।
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् ॥
अर्थ:
जो व्यक्ति धन-धान्य के लेन-देन में, विद्या अथवा किसी कला को सीखने में, भोजन के समय अथवा व्यवहार में लज्जाहीन होता है, अर्थात् संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। ॥ 2॥
व्यक्ति को लेन-देन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी बात स्पष्ट और साफ शब्दों में कहनी चाहिए। विद्या अथवा किसी गुण को सीखते समय संकोच करने से भी हानि होती है।
इसी प्रकार भोजन करते समय जो व्यक्ति संकोच करता है, वह भूखा रह जाता है, इसीलिए भोजन के समय, लोकाचार और व्यवहार के समय व्यक्ति को संकोच न करके अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने चाहिए। लोग श्लोक के आखिरी वाक्य को उद्धृत कर कहते हैं कि ‘निर्लज्ज सुखी होता है।’ संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ करना चाहिए ताकि अर्थ का अनर्थ न हो।
सन्तोषाऽमृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम् ।
न च तद् धनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥
अर्थ:
जो व्यक्ति संतोषरूपी अमृत से तृप्त है, मन से शांत है, उसे जो सुख प्राप्त होता है, वह धन के लिए इधर-उधर दौड़-धूप करने वाले को कभी प्राप्त नहीं होता। ॥3॥
संतोष की बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति संतोष से अपना जीवन बिताते हैं और शांत रहते हैं, उन्हें जितना सुख प्राप्त होता है, वह धन के लालच के लिए हर समय दौड़-धूप करने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। संकेत है कि लोभी से संतोषी श्रेष्ठ है और संतोष जीवनदाता है।
सन्तोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने।
त्रिषु चैव न कर्तव्योऽध्ययने तपदानयोः ॥
अर्थ:
अपनी पत्नी, भोजन और धन- इन तीनों के प्रति मनुष्य को संतोष रखना चाहिए, परंतु विद्याध्ययन, तप और दान के प्रति कभी संतोष नहीं करना चाहिए। ॥4॥
चाणक्य के अनुसार, व्यक्ति को अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना चाहिए, अन्य स्त्रियों से संबंध बनाना अपमानित करता है। व्यक्ति को घर में जो भोजन प्राप्त होता है और उसकी जितनी आय है उसमें ही संतोष करना चाहिए लेकिन विद्या के अध्ययन, यम-नियमों आदि के पालन और दान आदि कार्यों से कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए अर्थात व्यक्ति जितना अधिक अध्ययन करेगा, जितना अधिक अपने चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए तप करेगा तथा दान आदि करता रहेगा, उससे मनुष्य को लाभ होगा। ये तीन चीजें ऐसी हैं, जिनसे मनुष्य को संतोष नहीं करना चाहिए। संतुष्टि कहां हो और कहां नहीं, जीवन में यह जानना भी जरूरी है।(Chanakya Niti chapter 7)
यहां एक क्लिक में पढ़े ~ चाणक्य नीति : प्रथम अध्याय
विप्रयोर्विप्रवन्योश्च दम्पत्योः स्वामिभृत्ययोः ।
अन्तरेण न गन्तव्यं हलस्य वृषभस्य च ॥
अर्थ:
दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और अग्नि के बीच से, पति-पत्नी के बीच से, सेवक और नौकर के बीच से तथा हल-बैल के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए। ॥5॥
जहां दो ब्राह्मण खड़े हों या बात कर रहे हों, उनके बीच से नहीं निकलना चाहिए। इससे उनका अपमान होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण और अग्नि के बीच से निकलकर नहीं जाना चाहिए, हो सकता है कि ब्राह्मण हवन, यज्ञ आदि कर रहा हो।
इसी प्रकार पति-पत्नी जहां कहीं खडे अथवा बैठे हों, उनके बीच से निकलना भी अनुचित माना गया है। मालिक और नौकर, हल और बैल-इन दोनों के बीच से भी नहीं निकलना चाहिए, हो सकता है कि मालिक और नौकर किसी विशेष बात पर चर्चा कर रहे हों। हल और बैल के बीच में से निकलने का भाव बिलकुल स्पष्ट है कि ऐसे में चोट लग सकती है।
पादाभ्यां न स्पृशेदग्निं गुरुं ब्राह्मणमेव च।
नैव गं न कुमारीं च न वृद्धं न शिशुं तथा॥
अर्थ:
अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़ा आदमी और छोटे बच्चे- इन सबको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। ॥6॥
कुछ कार्य ऐसे भी हैं, जिन्हें करने से हानि होती है और कुछ कार्य आचार-व्यवहार के विपरीत होते हैं, उन्हें करने से समाज में अपयश होता है। अग्नि को पवित्र माना गया है, इसलिए उसे पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण और गाय को भी पूज्य होने के कारण पैर से छूना उचित नहीं। कुंवारी लड़की, बूढ़े आदमी और बच्चे भी सम्मान के पात्र होते हैं, इसलिए इन्हें भी पैर से नहीं छूना चाहिए। पूज्य को यथायोग्य सम्मान देने पर यदि आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है, तो अनादर करने से इनकी हानि भी तो होगी ही। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनसे इस कथन की पुष्टि होती है।
शकटं पञ्चहस्तेन दशहस्तेन वाजिनम्।
हस्ती शतहस्तेन देशत्यागेन दुर्जनम् ॥
अर्थ:
बैलगाड़ी से पांच हाथ, घोड़े से दस हाथ और हाथी से सौ हाथ दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। लेकिन दुष्ट से बचने के लिए यदि स्थान विशेष का त्याग भी करना पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए। ॥7॥(Chanakya Niti chapter 7)
व्यक्ति को स्वयं इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि किसी कारणवश उसे हानि न पहुंचे। बैलगाड़ी के बिलकुल निकट चलने से कोई दुर्घटना हो सकती है। घोड़ा किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है। हाथी से भी कुचले जाने का भय रहता है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि दुष्ट व्यक्ति इन सबसे बुरा होता है। इन सबसे बचने का यदि कोई और उपाय न हो तो व्यक्ति को स्वयं वह स्थान विशेष त्याग देना चाहिए।
हस्ती अंकुशमात्रेण वाजी हस्तेन ताड्यते।
शृंगी लगुडहस्तेन खड्गहस्तेन दुर्जनः ॥
अर्थ:
हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है। घोड़े को हाथ की थाप से सीधे रास्ते पर लगाया जाता है। सींग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से मारा जाना चाहिए क्योंकि वह वश में नहीं आता, उसे नष्ट ही करना होता है। ॥8॥
तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा घनगर्जिते ।
साधवः परसम्पत्तौ खलः परविपत्तिषु ॥
अर्थ:
ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है, मोर बादलों के गर्जने पर, सज्जन दूसरे को संपन्न और सुखी देखकर परंतु दुष्ट दूसरों को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। ॥9॥
आचार्य चाणक्य ने यहां स्वभाव की ओर संकेत किया है। भोजन करके ब्राह्मण संतुष्ट होता है, क्योंकि इससे उसे खिलाने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है। बादलों को जल से भरा और प्रसन्नता के कारण गर्जना करता देखकर मयूर नृत्य करने लगता है। इसी तरह सज्जन दूसरों को सुखी देखकर हर्ष का अनुभव करते हैं, जबकि दुष्ट दूसरे के दुख में सुखी होते हैं।
आचार्य ने दुष्ट और सज्जन के स्वभाव के अंतर से यह बताना चाहा है कि प्रत्येक को स्वयं में झांककर देखना चाहिए कि वह दूसरों के सुख में सुख का अनुभव कर रहा है या उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में या दुखी देखने में सुख की अनुभूति होती है। पहली स्थिति सज्जन की है और दूसरी दुष्ट व्यक्ति की।
अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन दुर्जनम्।
आत्मतुल्यबलं शत्रु विनयेन बलेन वा॥
अर्थ:
बलवान शत्रु को अनुकूल तथा दुर्जन शत्रु को प्रतिकूल व्यवहार द्वारा अपने वश में करें। इसी प्रकार अपने समान बल वाले शत्रु को विनम्रता या बल द्वारा, जो भी उस समय उपयुक्त हो, अपने वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। ॥10॥
चाणक्य का कहना है कि समय और स्थिति के अनुसार अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु बलवान है तो विनयपूर्वक उसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए अथवा अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दुष्ट शत्रु के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना चाहिए क्योंकि सज्जनतापूर्वक किए गए व्यवहार को वह कमजोरी समझेगा, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उसकी दुष्टता पर अंकुश लगे।(Chanakya Niti chapter 7)
बाहुवीर्य बलं राज्ञो ब्राह्मणो ब्रह्मविद् बली।
रूपयौवनमाधुर्य स्त्रीणां बलमुत्तमम् ॥
अर्थ:
राजा का बल अथवा शक्ति उसकी भुजाओं का बल है। ब्राह्मण का बल उसका ज्ञान है और स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ-साथ उनका सुमधुर व्यवहार है। ॥11॥
राजा के भुजबल से चाणक्य का भाव उसकी सशक्त सेना से है, जिस राजा की सेना सशक्त होगी, वह देश की रक्षा कर सकेगा परंतु इसके साथ साथ शारीरिक रूप से राजा को स्वयं भी बलवान होना चाहिए। वह सेना की प्रेरणा होता है। ब्राह्मण की शक्ति ईश्वर संबंधी ज्ञान है। स्त्रियों का बल रूप और यौवन के साथ-साथ उनका मधुर व्यवहार है। इन दोनों का समन्वय यदि न हो, तो स्त्री उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती जितनी कि उसमें संभावना है।
यहां एक क्लिक में पढ़ें ~ चाणक्य मंत्र हिंदी में
नाऽत्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीम्।
छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः ॥
अर्थ:
मनुष्य को अत्यन्त सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े-मेढ़े गांठों वाले वृक्ष खड़े रहते हैं। ॥12॥
आचार्य चाणक्य के अनुसार, मनुष्य को अत्यन्त सरल और सीधे-स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। इससे उसे सब लोग दुर्बल और मूर्ख मानने लगते हैं तथा हर समय कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं। सीधा सादा व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के के लिए सुगम होता है जबकि टेढ़े व्यक्ति से सब बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दुरुपयोग तो होगा ही।
यत्रोदकं तत्र वसन्ति हंसाः तथैव शुष्कं परिवर्जयन्ति ।
यत्रोदकं तत्र वसन्ति हंसाः तथैव शुष्कं परिवर्जयन्ति ।
न हंसतुल्येन नरेण भाव्यं पुनस्त्यजन्ते पुनराश्रयन्ते ॥
अर्थ:
जहां जल रहता है, वहां हंस रहते हैं और जब जल सूख जाता है तो हंस उस स्थान को छोड़ देते हैं। मनुष्य को हंस के समान स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे कभी त्याग करते हैं और कभी आश्रय लेते हैं। ॥13॥
मनुष्य ही नहीं देवता भी स्वार्थी हैं। जब तक कोई स्तुति करता है, संबंध रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन चाणक्य इसे ठीक नहीं मानते। उनका मानना है कि सुख में ही नहीं, दुख में भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यदि किसी ने समय पर आपके लिए कुछ किया है तो। ऐसा नीति की दृष्टि से भी आवश्यक है। संबंधों को तोड़ना बुद्धिमान व्यक्ति का स्वभाव या गुण नहीं है। कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। अगर संबंध ही तोड़ दिया, तो आप उसके पास फिर किस मुंह से जाएंगे।
उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्।
तडागोदरसंस्थानां परीवाह इवाऽम्भसाम् ॥
अर्थ:
अर्जित अथवा कमाए हुए धन का त्याग करना अर्थात् उसका ठीक ढंग से व्यय करना, उससे सार्थक लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को निकालते रहने से ही उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र रहता है। ॥14॥(Chanakya Niti chapter 7)
मनुष्य द्वारा कमाए गए धन का सही उपयोग यही है कि वह उसे ठीक ढंग से काम में लाए। उसका दान करे, उसका उचित उपभोग करे- सही अर्थों में यही धन की रक्षा है। यदि धन कमाने के बाद उसका सही उपयोग नहीं किया जाएगा तो धन कमाने का लाभ ही क्या है? यह बात उसी प्रकार ठीक है जैसे यदि तालाब में भरे हुए पानी को निकाला नहीं जाएगा तो वह सड़ जाएगा। सड़ने से बचाने के लिए उसका उपयोग आवश्यक है। इसी तरह तालाब की रक्षा हो सकती है। धन की रक्षा का भी उपाय यह है कि उसका सदुपयोग किया जाए।
यस्याऽर्थास्तस्य मित्राणि यस्याऽर्थास्तस्य बान्धवाः।
यस्याऽर्थाः स पुमांल्लोके यस्याऽर्थाः स च जीवति ॥
अर्थ:
संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के सब भाई-बन्धु और स्वजन होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार वह आदरपूर्वक अपना जीवन बिताता है। ॥15॥
आचार्य ने धन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यहां स्पष्ट किया है कि मनुष्य के पास जब तक धन रहता है, तब तक सब उसके मित्र बने रहते हैं। जिसके पास धन होता है, उसके रिश्तेदार भी बहुत होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है और धनवान व्यक्ति का ही जीवन धन्य कहलाने योग्य है। निर्धन व्यक्ति तो निर्जीव के समान है क्योंकि न तो उसकी ओर कोई ध्यान देता है, न ही कोई उसका अपना होता है।
धन में ऐसी शक्ति है कि यह जानते हुए भी कि यह आने-जाने वाला है सब लोग धनवान व्यक्ति को ही अपना मित्र और पारिवारिकजन बनाना उचित समझते हैं, उसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है।
स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे।
दानप्रसंगो मधुरा च वाणी देवाऽर्चनं ब्राह्मणतर्पणं च॥
अर्थ:
स्वर्ग से इस संसार में आने वाले जीव के शरीर में चार बातें उसके चिह्न रूप में रहती हैं अर्थात् उसके चार प्रमुख गुण होते हैं। उसमें दान देने की प्रवृत्ति होती है। वह मधुरभाषी होता है। देवताओं की पूजा-अर्चना करता है, उनका आदर-सत्कार करता है और विद्वान-ब्राह्मणों को सदैव तृप्त अर्थात् संतुष्ट रखता है। ॥16॥
आचार्य चाणक्य के अनुसार, जिन व्यक्तियों में ये चार गुण होते हैं। वे मानो पृथ्वी पर उतरे हुए देवता ही हैं। वाणी में मिठास, प्रेमपूर्वक बिना अभिमान के बात करना, दान देने की प्रवृत्ति, देवताओं का आदर-सत्कार और उनकी पूजा-अर्चना करना तथा ब्राह्मणों को पूजा तथा आदर-सम्मान द्वारा तृप्त करने का प्रयत्न करना ही तो देवताओं के लक्षण हैं। इसे धर्मग्रंथों में दैवी संपत्ति कहते हैं।
अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्।
नीचप्रसंगः कुलहीनसेवा चिह्नानि देहे नरकस्थितानाम् ॥
अर्थ:
(इसी प्रकार) नरक में रहने वाले जब देह धारण कर इस संसार में आते हैं तो उनमें ऊपर बताए गए चिह्नों के सर्वथा विपरीत चिह्न होते हैं। वे मधुरभाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। कड़वी बात कहते हैं। वे निर्धन होते हैं। अपने परिवारजनों तथा मित्रों से वे द्वेष-भाव रखते हैं। उनकी संगति में नीच लोग रहते हैं और वे नीच कुल वालों की सेवा करते हैं। ॥17॥
यह श्लोक पूर्व श्लोक के भाव से संबंधित है। दुष्ट लोग अत्यन्त क्रोधी स्वभाव के होते हैं। मधुर भाषण करने के बजाय कठोर और कड़वी बातें बोलते हैं। वे दरिद्र होते हैं अर्थात उनके पास धन नहीं होता। जिस प्रकार कुत्ता दूसरे अपरिचित कुत्ते को देखकर उस पर भौंकता है, उसी प्रकार दुष्ट अपनों से भी वैर-भाव रखने लगता है। उसके संगी-साथी नीच होते हैं और वह नीच लोगों की ही सेवा करता है। ऐसे लोग नरक से आते हैं और जहां रहते हैं वहां भी नरक ही बना देते हैं।
गम्यते यदि मृगेन्द्र-मन्दिरं लभ्यते करिकपोलमौक्तिकम्।
जम्बुकाऽऽलयगते च प्राप्यते वत्स-पुच्छ खर-चर्म-खण्डनम् ॥
अर्थ:
यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो वहां संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती (गजमुक्ता) प्राप्त हो जाए लेकिन यदि कोई गीदड़ की गुफा में जाएगा तो वहां उसे किसी बछड़े की पूंछ का अथवा गधे की खाल का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। ॥18॥
इस श्लोक से चाणक्य का भाव यह है कि साहसी और शूरवीर व्यक्ति की संगति में यद्यपि भय और खतरा है, फिर भी वहां रत्नों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु दुष्ट, कायर और ठग व्यक्ति के पास तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, कुछ मिलता भी है, तो वह तुच्छ तथा निकृष्ट होता है।(Chanakya Niti chapter 7)
शुनः पुच्छमिव व्यर्थ जीवितं विद्यया विना।
न गुह्यगोपने शक्तं न च दंशनिवारणे ॥
अर्थ:
विद्या के बिना मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है, जिससे न तो वह अपने शरीर के गुप्त भागों को ढक सकता है और न ही काटने वाले मच्छरों आदि को उड़ा सकता है। ॥9॥
वाचः शौचं च मनसः शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
सर्वभूते दया शौचं एतच्छौत्रं पराऽर्थिनाम् ॥
अर्थ:
वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणिमात्र पर दया, धन की पवित्रता, मोक्ष प्राप्त करने वाले के लक्षण होते हैं। ॥20॥
नीति ग्रंथों में अध्यात्म से संबंधित श्लोकों का आना कुछ पाठकों को खटक सकता है। उन्हें ऐसा लगेगा मानो आचार्य अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। लेकिन ऐसा समझना आचार्य चाणक्य के व्यक्तित्व को न समझ पाना है। अपनी कूटनीतिक चालों से शत्रु को मात देने वाले आचार्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इसीलिए सफल हुए क्योंकि वे अपने अंतरमन से उतने सरल और सहज थे। महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लघु स्वार्थों को छोड़ने की उन्होंने शिक्षा ही नहीं दी, उन्हें अपने आचरण में भी विशिष्ट स्थान दिया। अध्यात्म उनके जीवन का आधार था। बंधन तो लीला मात्र है, असल में तो उनके सारे प्रयास मुक्ति के लिए ही थे।
उन्होंने इन श्लोकों द्वारा बताया कि भगवत्ता और दिव्यता कहीं अन्यत्र नहीं हैं। प्रत्येक में वह रची-बसी है। जरूरत है उसका अनुभव करने की। आचार्य ने उस अनुभव के लिए शुचिता (पवित्रता) को सबसे आवश्यक माना है। जो वाणी और मन से पवित्र होगा और जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी होता होगा वही विवेकवान् हो सकता है।
परोपकार की भावना हो, लेकिन इंद्रियों पर संयम न हो, तो भी अपने लक्ष्य को पाया नहीं जा सकता। एक स्थिति प्राप्त करने के बाद मार्ग से भटकने का भय बना रहता है। संयमी तो वहां स्वयं को संभाल लेता है, जहां इंद्रिय लोलुप उलझ जाता है। बिना विवेक के सत्य का ज्ञान नहीं होता और उसके बिना बंधनमुक्त भी नहीं हुआ जा सकता।
पुष्पे गन्धं तिले तैलं काष्ठेऽग्निं पयसि घृतम्।
इक्षौ गुडं तथा देहे पश्याऽऽत्मानं विवेकतः ॥
अर्थ:
जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी और ईख में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक का सहारा लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ॥21॥(Chanakya Niti chapter 7)
आचार्य ने साधन और साध्य दोनों का स्पष्ट कथन किया है यहां।
यहां एक क्लिक में पढ़ें ~ श्रीमद भागवत गीता का प्रथम अध्याय
अध्याय का सार:
मनुष्य को कई कारणों से धन की हानि होती है। कई कारणों से वह दुखी रहता है। परिवार में कभी कुछ दोष भी आ जाते हैं तथा कई बार उसे धूर्त लोगों के हाथों से धोखा भी उठाना पड़ता है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को ऐसी बातों को किसी दूसरे पर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा करने से जगहंसाई के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है।
जो मनुष्य लेन-देन के संबंध में संकोच करता है, उसे हानि उठानी पड़ती है। किसी विद्या की प्राप्ति अथवा कोई गुण सीखते समय भी मनुष्य को संकोच नहीं करना चाहिए। यहां संकोच न करने का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अत्यंत लोभी हो जाए। मनुष्य को संतोषी होना चाहिए, परंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके संबंध में संतोष करने से हानि होती है, जैसे – विद्या, प्रभु स्मरण और दान आदि।
यहां आचार्य ने सामान्य आचरण की बातों का भी उल्लेख किया है क्योंकि इनसे व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। जहां दो मनुष्य बात कर रहे हों, उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार जब कोई ब्राह्मण हवन आदि कर रहा हो तो उसके बीच से गुजरना ठीक नहीं। हल और बैल के बीच में जो अंतर होता है, उसे बनाए रखना चाहिए। यदि उस बीच में आने का कोई प्रयत्न करेगा तो हल के (फाल) अगले तीखे भाग से घायल हो जाएगा। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृक्ष और बालक को पैर नहीं लगाना चाहिए। इन्हें पैर लगाने का अर्थ है उनका अपमान करना। उन्होंने यहां पर यह भी बताया है कि ब्राह्मण को यदि सम्मानपूर्वक भोजन आदि करवा दिया जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है। आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर मोर प्रसन्न होता है। साधु अथवा सज्जन लोग दूसरों का कल्याण होने से प्रसन्न होते हैं, परंतु दुष्ट आदमी दूसरे की भलाई नहीं देख सकता। उसे इससे कष्ट होता है।
चाणक्य ने जहां समय के अनुकूल आचरण करने की बात कही है, वहीं वे यह भी कहते हैं कि अपने से बलवान शत्रु को चतुरतापूर्वक अनुकूल व्यवहार करके प्रसन्न करना चाहिए और अपने से कमजोर दिखाई देने वाले शत्रु को भय दिखाकर वश में कर लेना चाहिए। इस प्रकार राजा में चतुरता, विनम्रता और बल का सम्मिश्रण होना चाहिए। ब्राह्मण को अपनी शक्ति वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान से बढ़ानी चाहिए जबकि स्त्रियों की शक्ति उनकी मधुर वाणी है।
चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अत्यन्त सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। सीधे व्यक्ति को सब अपने उपयोग में लाना चाहते हैं, जिससे उसे अकसर हानि ही होती है, क्योंकि उसके हित की चिंता किसी को नहीं होती।(Chanakya Niti chapter 7)
आचार्य के अनुसार व्यक्ति को सदैव अपना रूप नहीं बदलते रहना चाहिए और न ही अपना स्थान। वे कहते हैं कि केवल उसी धनी व्यक्ति का सम्मान समाज में होता है, जो उस धन का सदुपयोग करता है अर्थात अच्छे धन को कामों में लगाता है, क्योंकि जो अच्छे लोग इस संसार में आते हैं, उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है। जो कटु-भाषण नहीं करते, देवी-देवता तथा ईश्वर की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट रखते हैं- वस्तुतः वे ही श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले दुष्टों की श्रेणी में आते हैं।
चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को सदैव सज्जनों और अपने से उत्तम पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए अर्थात मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से संपर्क बनाए, तभी वह संसार में सफल हो सकता है। नीच लोगों के साथ रहने में सदैव हानि होती है।
जिस प्रकार फूलों में सुगंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में धी, ईख में गुड़ होने पर भी दिखाई नहीं देता अर्थात ये चीजें इन वस्तुओं में विद्यमान रहती हैं, परंतु उन्हें आंख से देखा नहीं जा सकता, इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है। इसे प्रकट करने के लिए विशेष और सुव्यवस्थित प्रयास अर्थात् विशेष प्रकार की निरंतर साधना आवश्यक है।


 Download the Mahakavya App
Download the Mahakavya App